भूमिका
शिक्षा मनोविज्ञान अन्तःविषयक आयाम का परिणाम है। आज इस आयाम का उपयोग अध्ययन विषयों में अधिक तीव्रता से किया जा रहा है, जिससे नये-नये अध्ययन क्षेत्रों का विकास हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं की जटिलताएँ बढ़ रहीं हैं और विषय के विशेषज्ञ अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिये अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों के विशेषज्ञों का सहयोग एवं सहायता लेते हैं। इस प्रकार जो नया ज्ञान प्राप्त होता है, वह एक नया अध्ययन क्षेत्र होता है।
शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालक का सम्पूर्ण विकास करना है। सम्पूर्ण विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की प्रक्रिया को बाल-केन्द्रित माना है। शिक्षा की प्रक्रिया, बालक की योग्यताओं एवं क्षमताओं के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षक को पाठ्यवस्तु के अतिरिक्त छात्रों के मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए तथा उस ज्ञान का उपयोग भी आना चाहिए। शिक्षा-मनोविज्ञान के उपयोग से शिक्षा की प्रक्रिया प्रभावशाली तथा सार्थक हो जाती है। बालक केन्द्रित शिक्षा ने मनोविज्ञान
के प्रत्यय, नियमों तथा सिद्धान्तों के उपयोग को महत्व दिया है। शिक्षा की प्रक्रिया को समझने तथा प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को तीन मूल प्रश्नों के उत्तरों को भली-भाँति समझना चाहिए। यह प्रश्न इस प्रकार हैं-
शिक्षा क्यों दी जाए? शिक्षा में क्या दिया जाए? शिक्षा कैसे दी जाए?
जो
इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, उसे अन्य क्षेत्रों के विषय-विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ती है। प्रथम प्रश्न ‘शिक्षा क्यों दी जाए’? का उत्तर एक दार्शनिक ही दे सकता है, क्योंकि जीवन दर्शन के सम्बन्ध में र्शन ही-बोध कराता है। शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण दर्शन ही करता है। इसलिए शिक्षा-दर्शन को शिक्षा में महत्व दिया जाता है।
द्वितीय प्रश्न ‘शिक्षा में क्या दिया जाए? का उत्तर एक समाजशास्त्री ही दे सकता है। शिक्षा बालक का समाजीकरण करती है। सामाजिक मानकों, परम्पराओं तथा आचरणों का बोध समाजशास्त्री ही करता है। समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं को शिक्षा द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, इसलिए शिक्षा में शिक्षा-समाजशास्त्र को सम्मिलित किया गया है।
तृतीय प्रश्न ‘शिक्षा कैसे दी जाए? इस सम्बन्ध में पुरानी कहावत है-जॉन लैटिन (John
Latin)। यहाँ जॉन का अर्थ है- ‘छात्र’ तथा लैटिन का अर्थ है- ‘पाठ्यवस्तु’ अर्थात् शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए और अपने शिष्य की क्षमताओं का समुचित बोध होना चाहिए, तभी शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। बालक के सम्बन्ध में बोध, मनोविज्ञान का विशेषज्ञ ही दे सकता है। इसलिए शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा मनोविज्ञान को महत्व दिया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान से शिक्षा की प्रक्रिया तीव्र तथा प्रभावशाली बन सकती है। छात्र की रुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप शिक्षा की प्रक्रिया का सृजन किया जा सकता है, परन्तु शिक्षा के उद्देश्यों को महत्व नहीं दिया जाता है।
















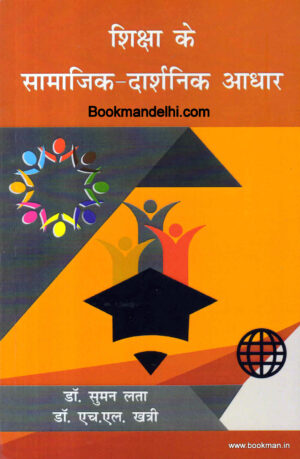

Reviews
There are no reviews yet.