आमुख
विश्व के मानचित्र में भारत अपनी जिन विशेषताओं के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखता है वह है, इसका सांस्कृतिक रूप से अति उन्नत होना और इस सांस्कृतिक उन्नति के मूल में सांगीतिक कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय जन मानस में संगीत कुछ इस तरह रचा-बसा हुआ है कि इसके बिना हम अपने किसी भी सांस्कृतिक या मांगलिक कार्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। आकाश में सूर्य किरणों के आगमन के साथ ही मंदिरों में आरती के स्वर गूंजने लगते हैं, तो गुरूद्वारों में कीर्तन, मस्जिदों में अजान के स्वर गूंजने लगते हैं, तो वहीं चर्च में यीशु के गीत आदि। सदियों से संगीत के सात स्वर मानव मन को अनुप्रागित करते हुए उसे अपनी भावनाएँ व्यक्त करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे हैं। संगीत हमारे समाज में वैदिक युग से व्याप्त है और आज भी इसकी प्रासांगिकता बनी हुई है। तभी तो कहा गया है- ‘नादाधीनम् जगत सर्वग्’।
भारतीय सांगीतिक कलाओं की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि हर समय, हर मौसम और हर अवसर पर यह अपनी सार्थकता सिद्ध करता है। अवसर चाहे स्वाधीनता दिवस समारोह का हो, दुर्गापूजा का हो या और कोई समारोह उस का सांस्कृतिक अवसर सांगीतिक स्वरों के बिना संपूर्ण हो ही नहीं सकता। भारत के कण-कण में संगीत व्याप्त है। इसका हर प्रांत, हर जिला संगीत के एक नये रूप से हमारा परिचय कराता है। इसी कारण राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कहा गया है कि संगीत माध्यमिक स्तर तक के बच्चों के लिए अनिवार्य होना चाहिए। सांगीतिक कलाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं आकर्षण बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास करता है। संगीत के शास्त्रीय एवं लोक पक्ष दोनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए, इसके पारंपरिक, मौलिक और सृजनात्मक पक्ष पर ध्यान देना आवश्यक है, जो हमारे संगीतार्थियों द्वारा ही संभव है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था- ‘सामवेद की ऋचाएँ संगीत की खदान हैं… कुरआन शरीफ़ की एक भी आयत बिना स्वर के नहीं कही जाती और ईसाई धर्म में डेविड के साम

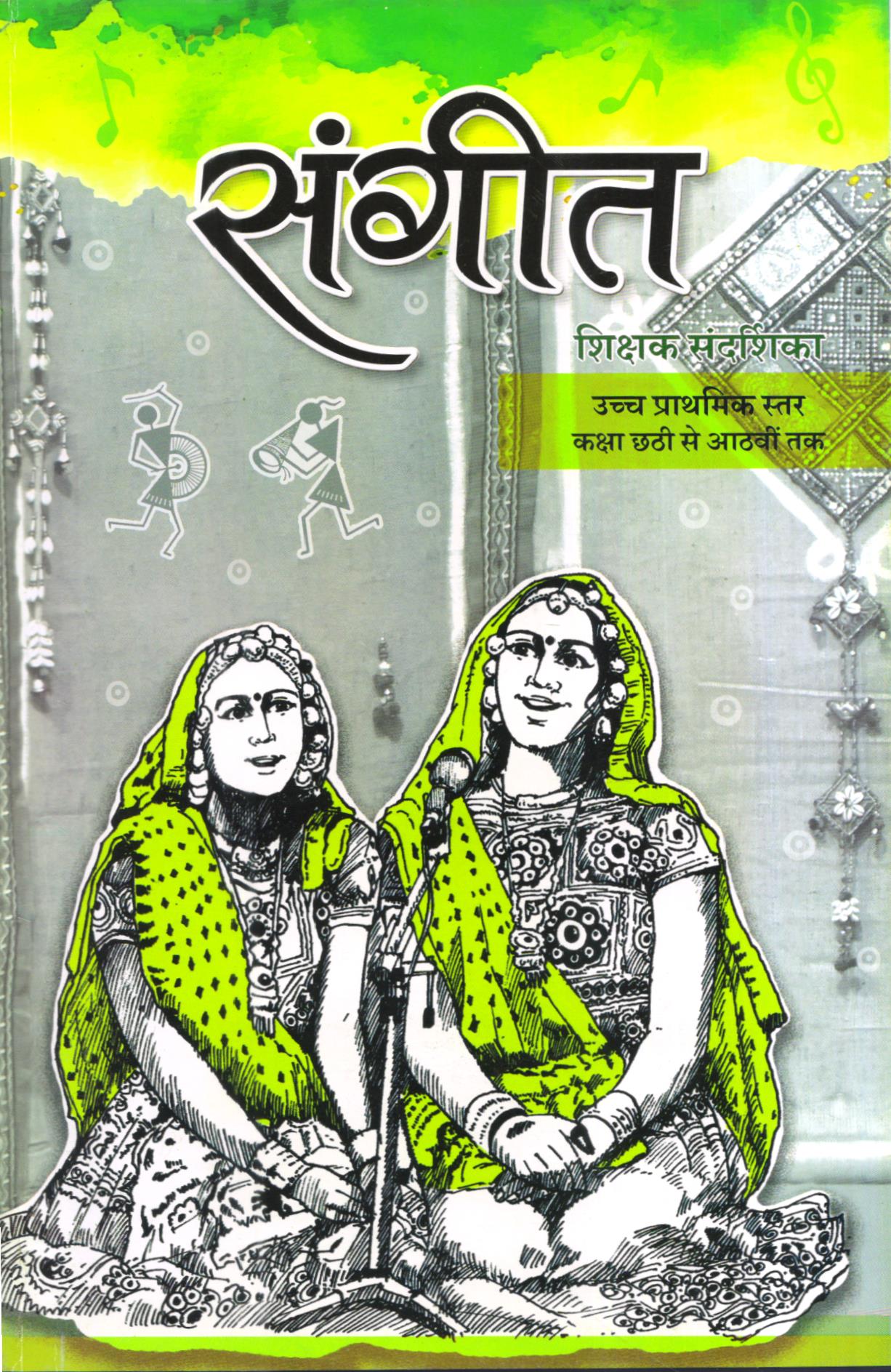
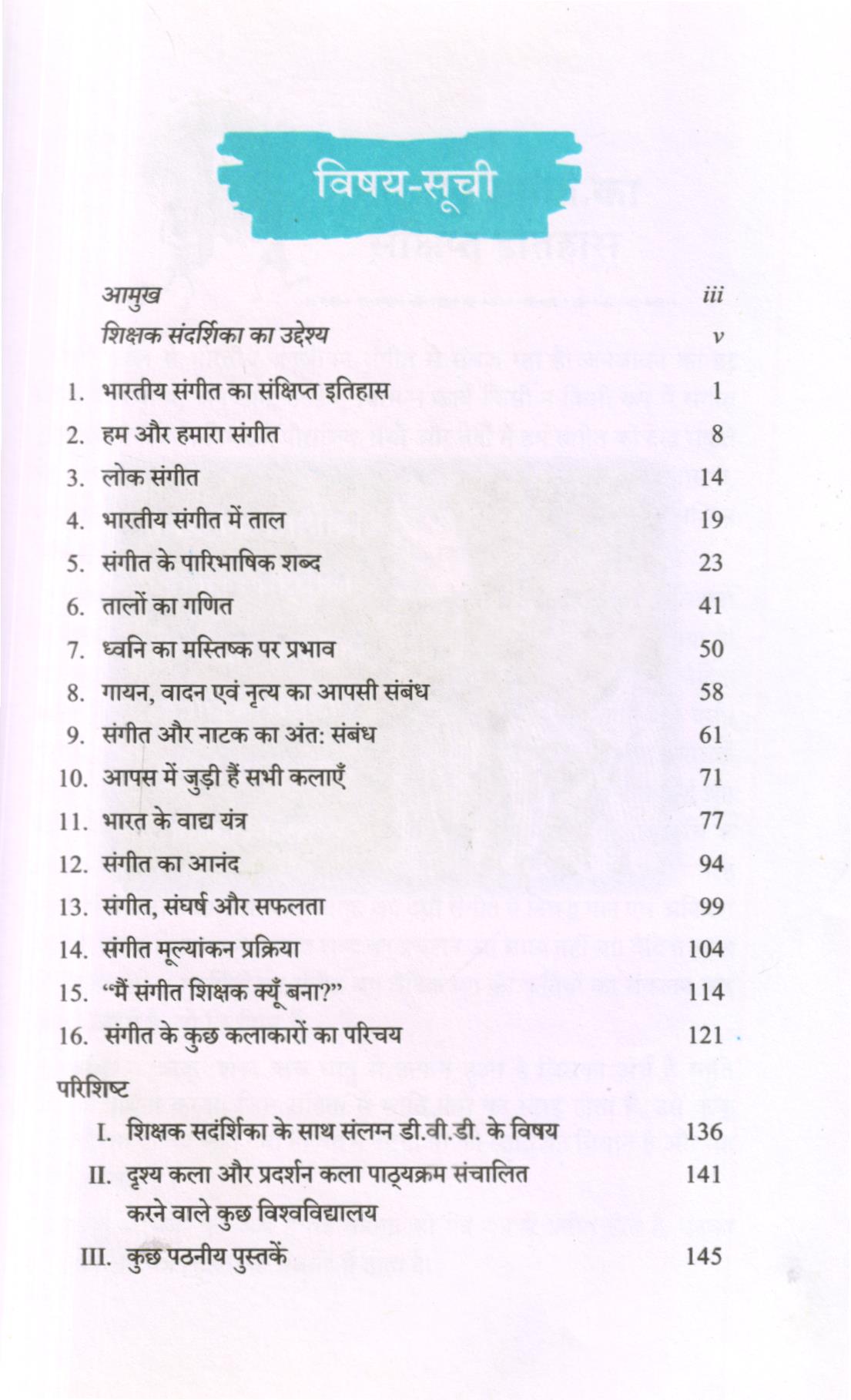
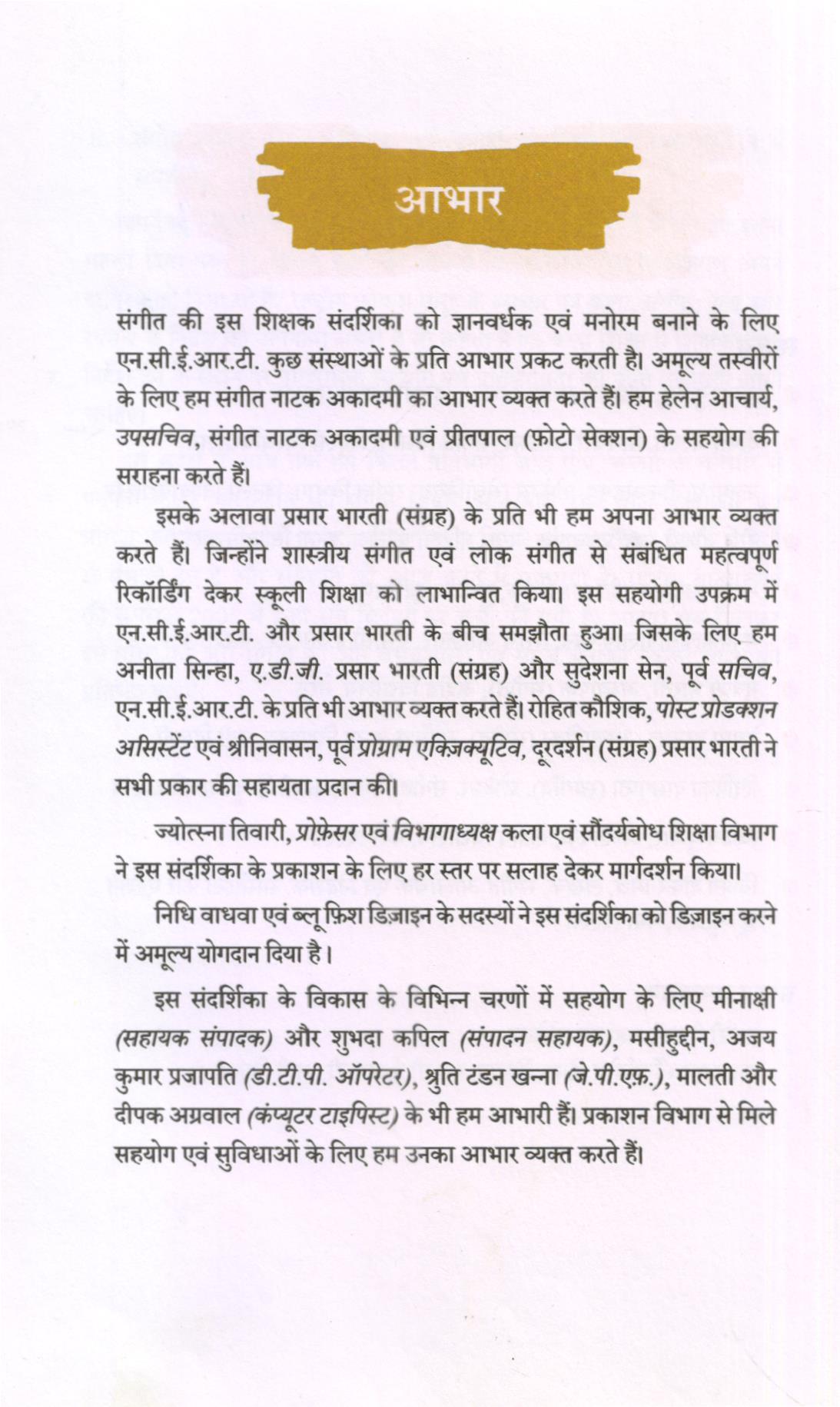
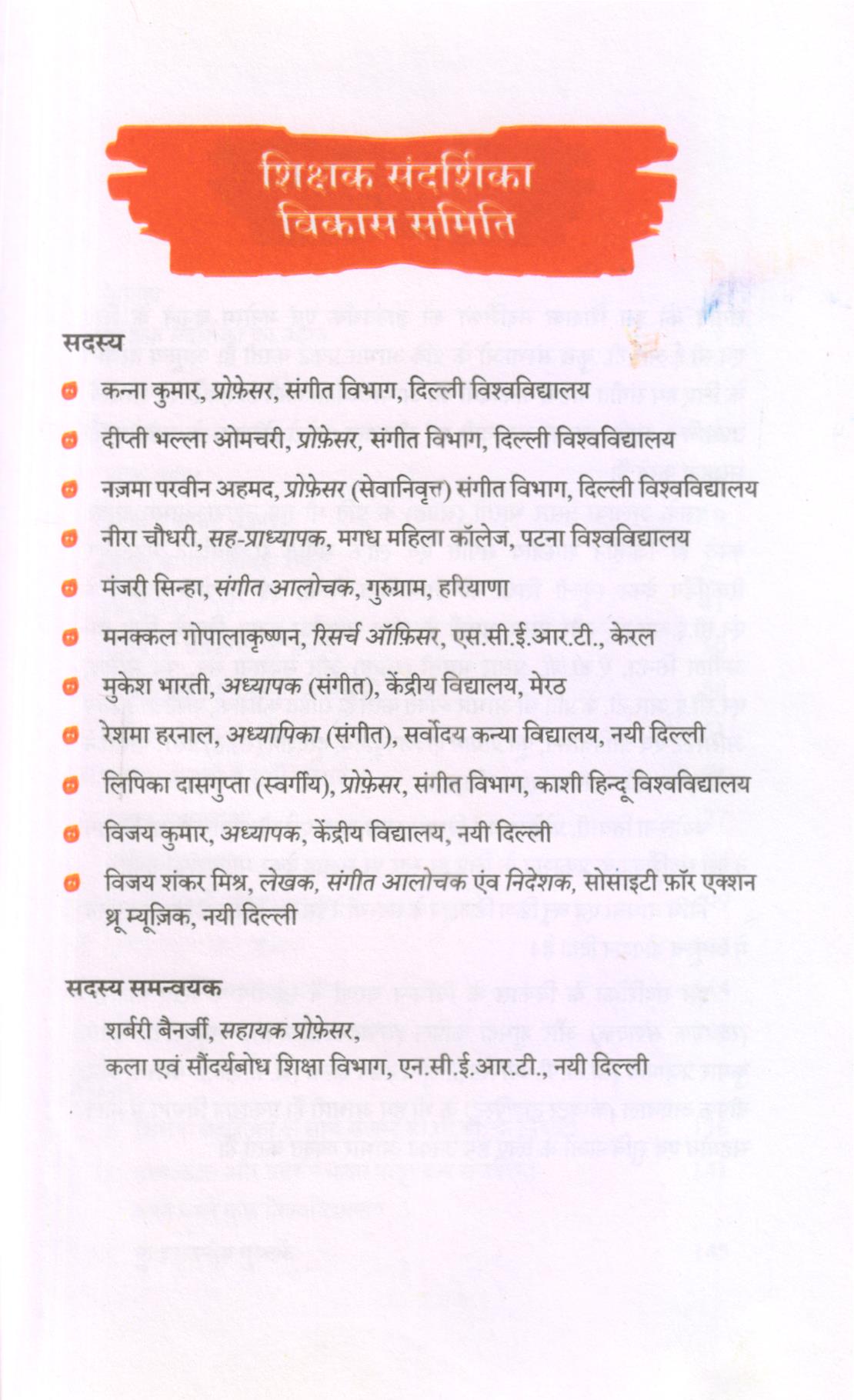
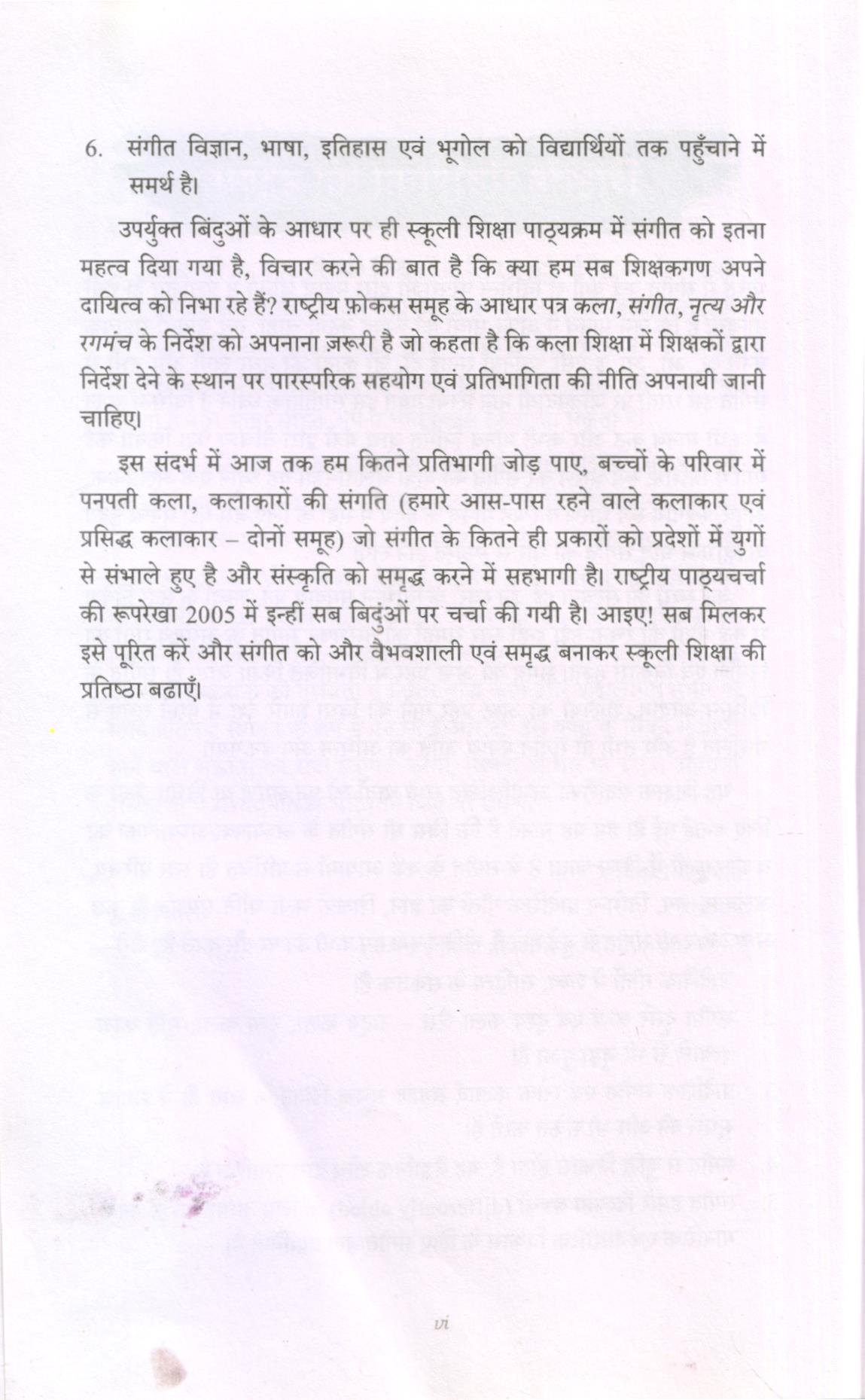
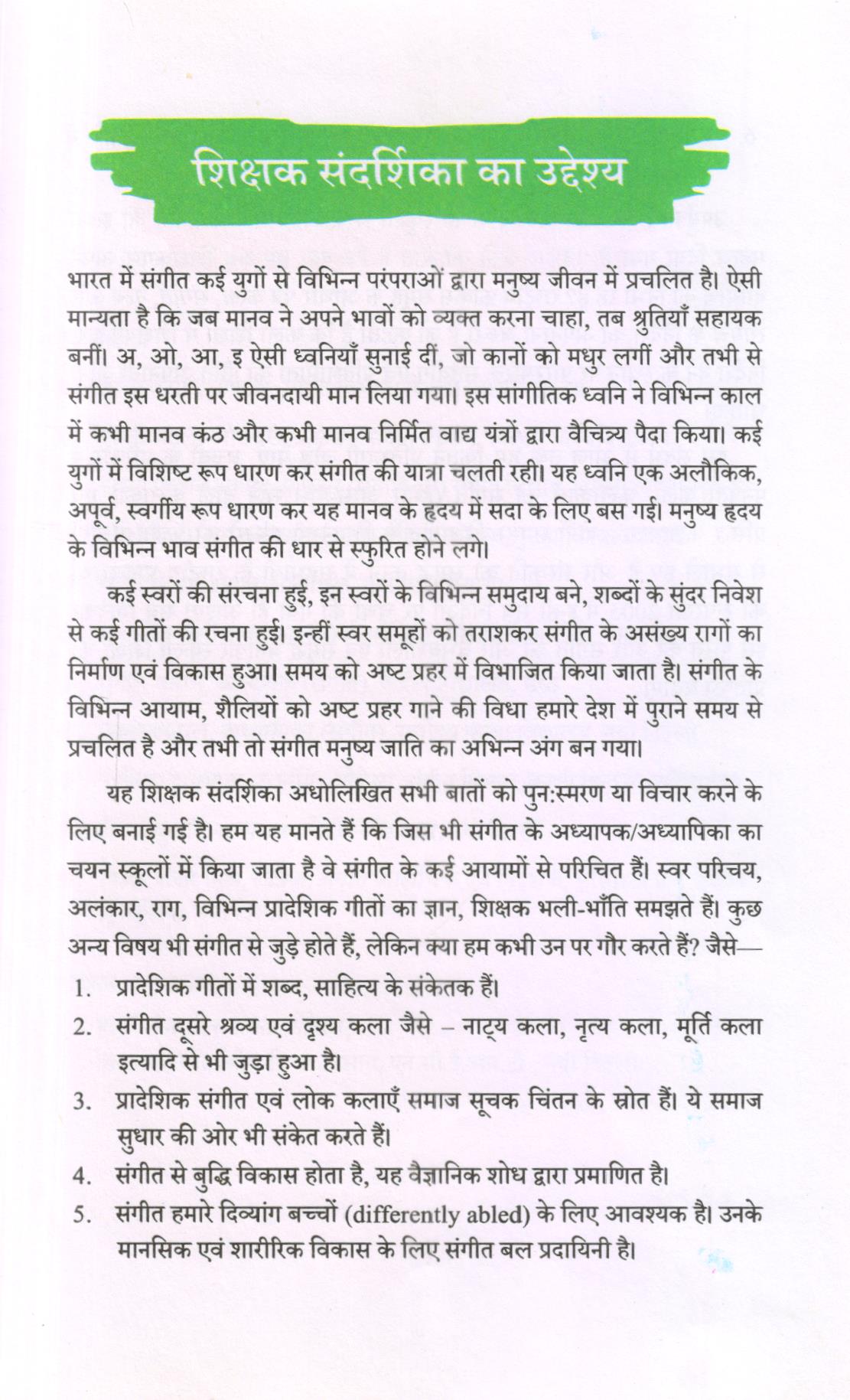
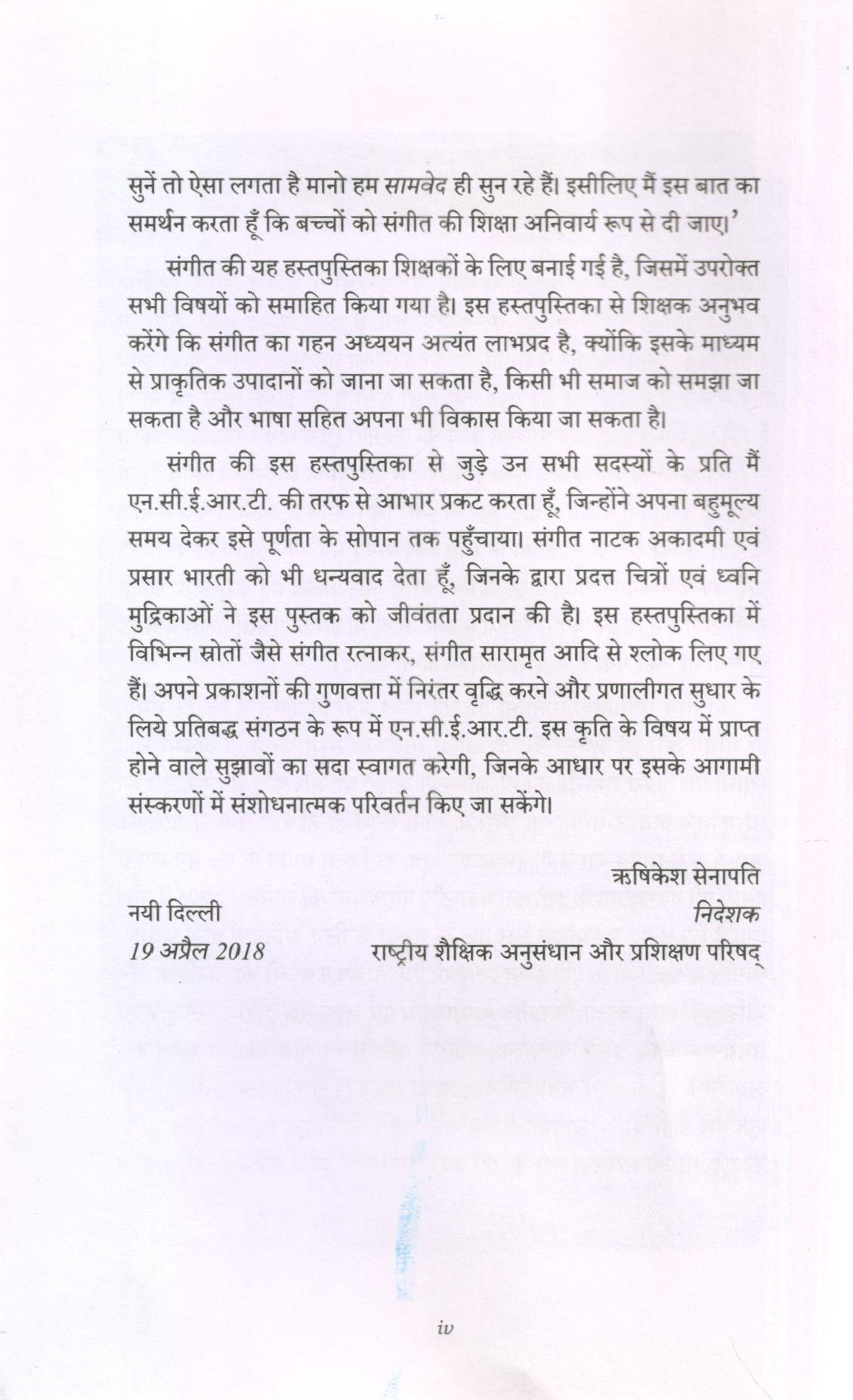
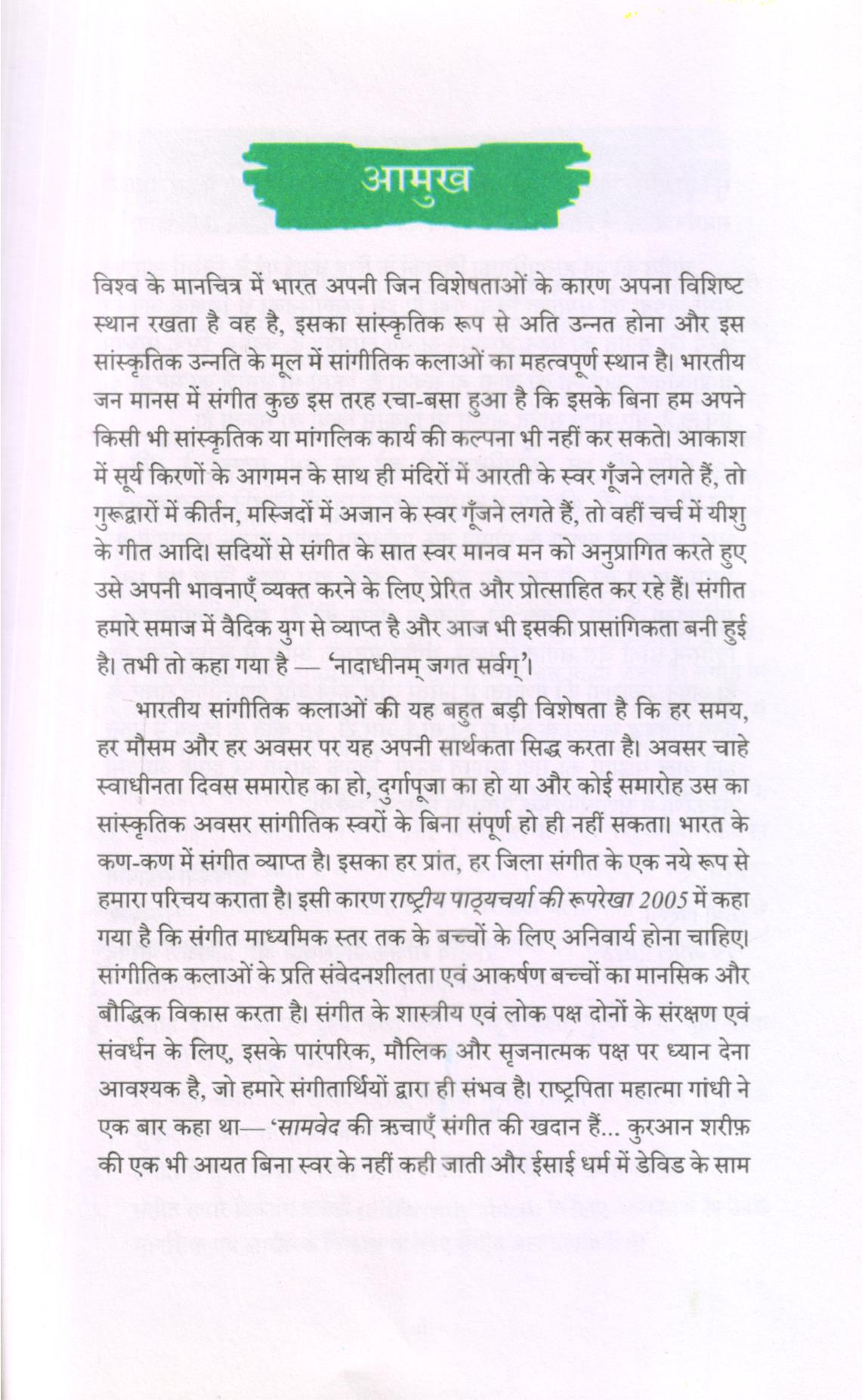




Reviews
There are no reviews yet.