भूमिका
दर्शन का इतिहास अधिक प्राचीन है। शायद धर्म के इतिहास का प्रारम्भ इसके पूर्व से होता है। फिर भी यह आश्चर्य की ही बात है कि आज तक इस मूल विषय के सम्बन्ध में ही सहमति नहीं है कि दर्शन का स्वरूप क्या है, उसकी ठीक-ठीक विषय-वस्तु क्या है? कम-से-कम पारम्परिक रूप में ऐसा माना गया है कि दर्शन विश्व तथा जीवन को उनकी समग्रता में समझने का एक प्रयास है। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। उसके सामने फैला विशाल विश्व तथा उसका अपना जीवन उसके सामने कुछ प्रश्न उपस्थित करते हैं जिन पर चिंतन करने के लिए वह बाध्य हो जाता है। ये प्रश्न या समस्याएँ विश्व या जीवन के किसी विशिष्ट पक्ष से सम्बन्धित नहीं होतीं। इनका सम्बन्ध विश्व तथा जीवन के कुछ ऐसे गहन तथा मूलभूत प्रश्नों से होता है जिनका एक व्यापक रूप में समग्र विश्व तथा समग्र जीवन से सम्बन्ध होता है। विश्व का मूलभूत स्वरूप क्या है? इसकी उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई? इसमें मनुष्य कैसे उत्पन्न हुआ। उसका इस विश्व में क्या स्थान है? आदि कुछ मूलभूत प्रश्न चिंतनशील मनुष्य को कठिनाई उत्पन्न करने लगते हैं और इन प्रश्नों पर सोचने के लिए वह बाध य हो जाते है। दर्शन मनुष्य के इसी प्रकार के चिन्तन की उपज है, वह ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर दूहुँने का प्रयास है। विश्व तथा जीवन के सम्बन्ध में ऐसा ही व्यापक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य दार्शनिक चिंतन प्रारम्भ करता है। ‘दर्शन’ के लिए जो अँगरेजी शब्द फिलॉसफी उसका शाब्दिक अर्थ है ‘ज्ञान के प्रति अनुराग’। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि दर्शन का प्रारम्भ जिज्ञासा से होता है और यह जिज्ञासा समग्र विश्व तथा समग्र-जीवन से सम्बन्धित कुछ मूलभूत प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने से उत्पन्न होती है। भारतीय-दर्शन की सामान्य विचारधारा को देखने से यह प्रतीत होता है कि इस दर्शन का प्रारम्भ दुःख से छुटकारा पाने के व्यवहारिक लक्ष्य से हुआ है, परन्तु इससे भारतीय दर्शन के स्वरूप में इस अर्थ में कोई भेद नहीं हो जाता कि वह दुःख से छुटकारा पाने का व्यवहारिक प्रयास है जबकि पाश्चात्य दर्शन विश्व को उसकी समग्रता में समझने का प्रयास है। दर्शन का उदगम स्प्रेत या लक्ष्य यहाँ भिन्न आवश्य है, परन्तु स्वरूप भिन्न नहीं है। यहाँ भी दर्शन विश्व तथा जीवन के स्वरूप को उनकी समग्रता में समझने का प्रयास ही है, भले इसका लक्ष्य दूसरा है। विश्व और जीवन के स्वरूप को भारतीय दर्शन में समझने की चेष्टा केवल जिज्ञासा की शान्ति के लिए नहीं, बल्कि दुःखों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। एक भेद पद्धति में भी है। पाश्चात्य दर्शन की पद्धति मुख्यतः बौद्धिक है। इसमें बौद्धिक तर्क-विर्तक, विचार-विमर्श के द्वारा यह समझने की चेष्टा की जाती है कि विश्व तथा जीवन का मौलिक स्वरूप क्या है?

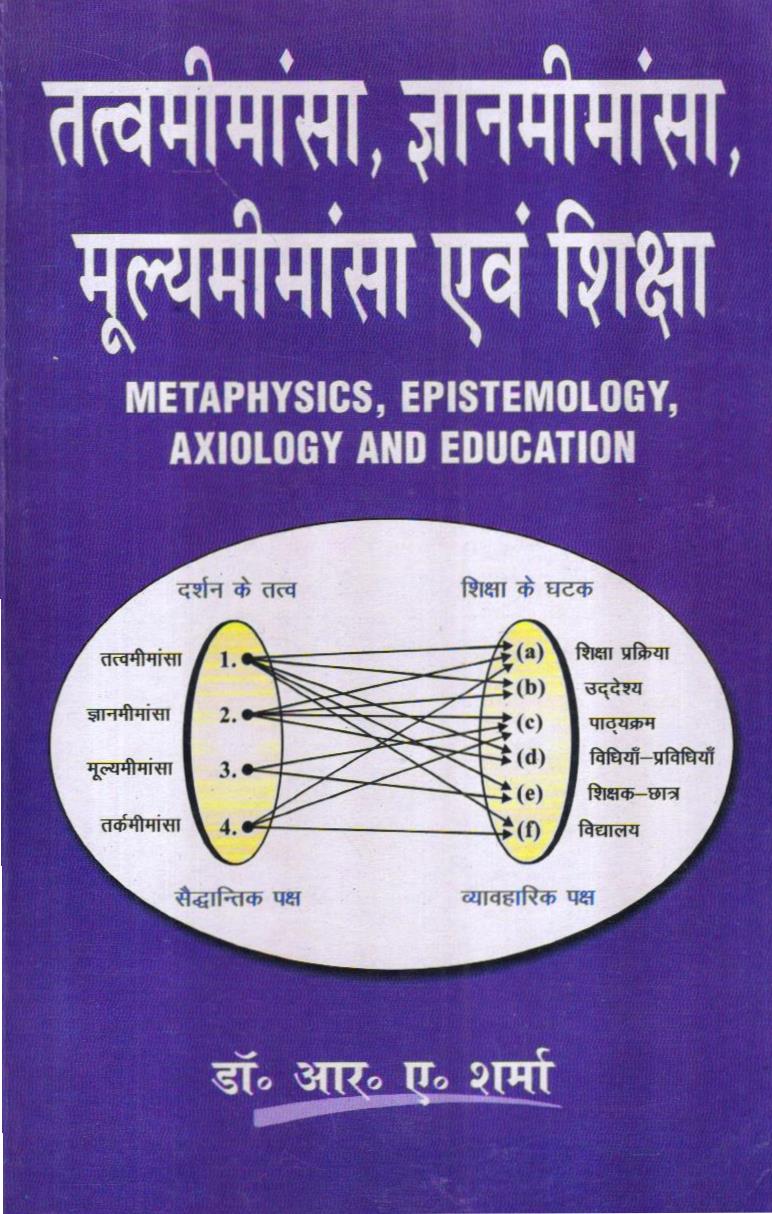
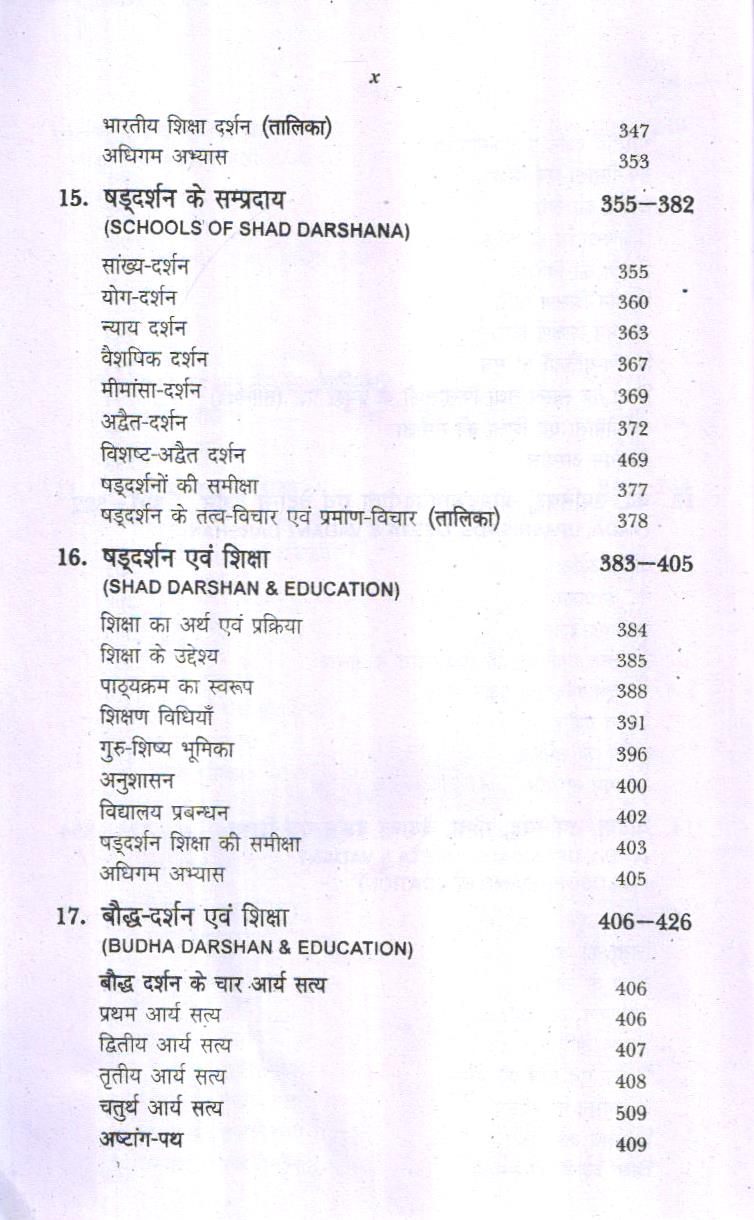
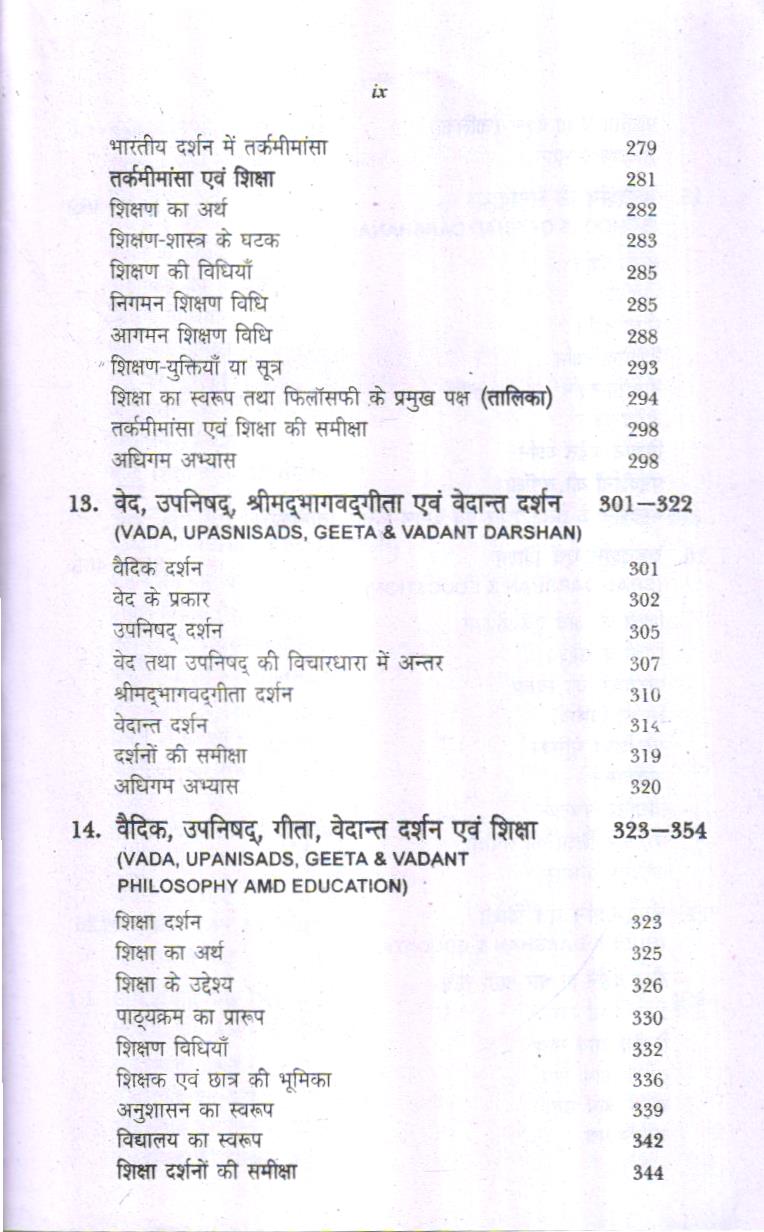
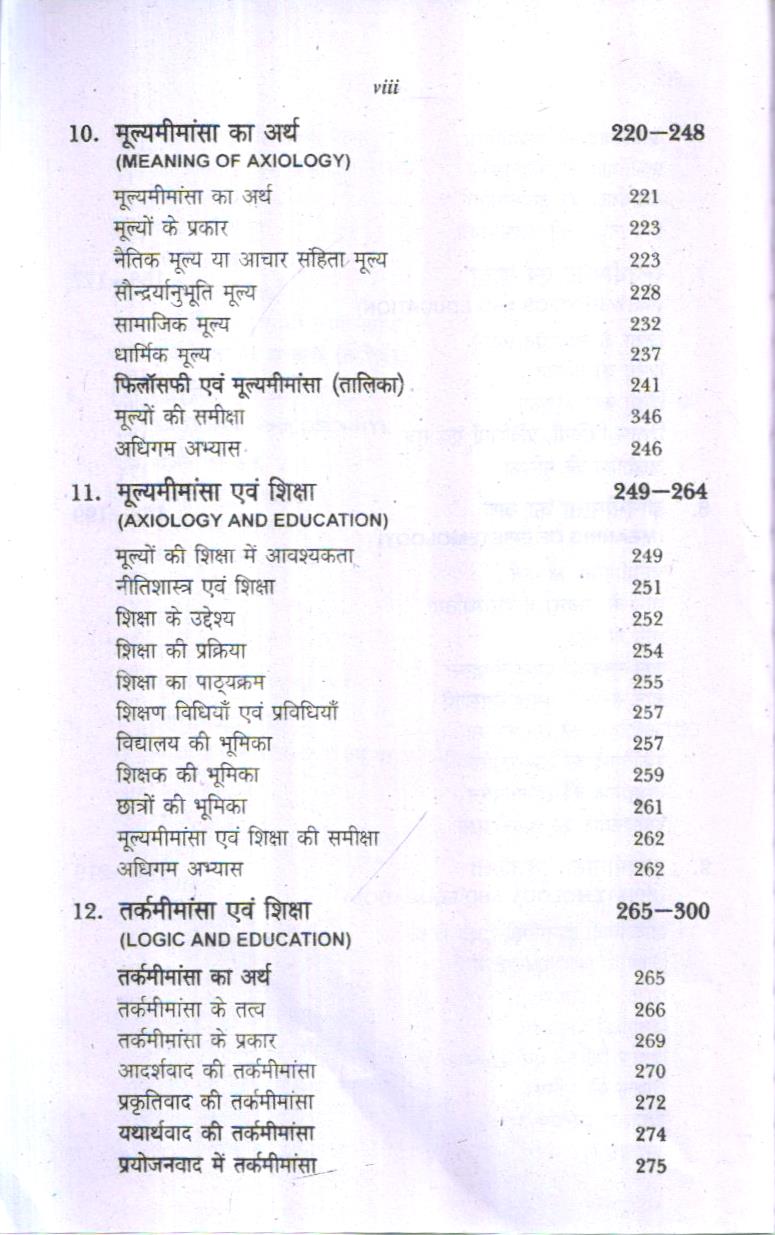
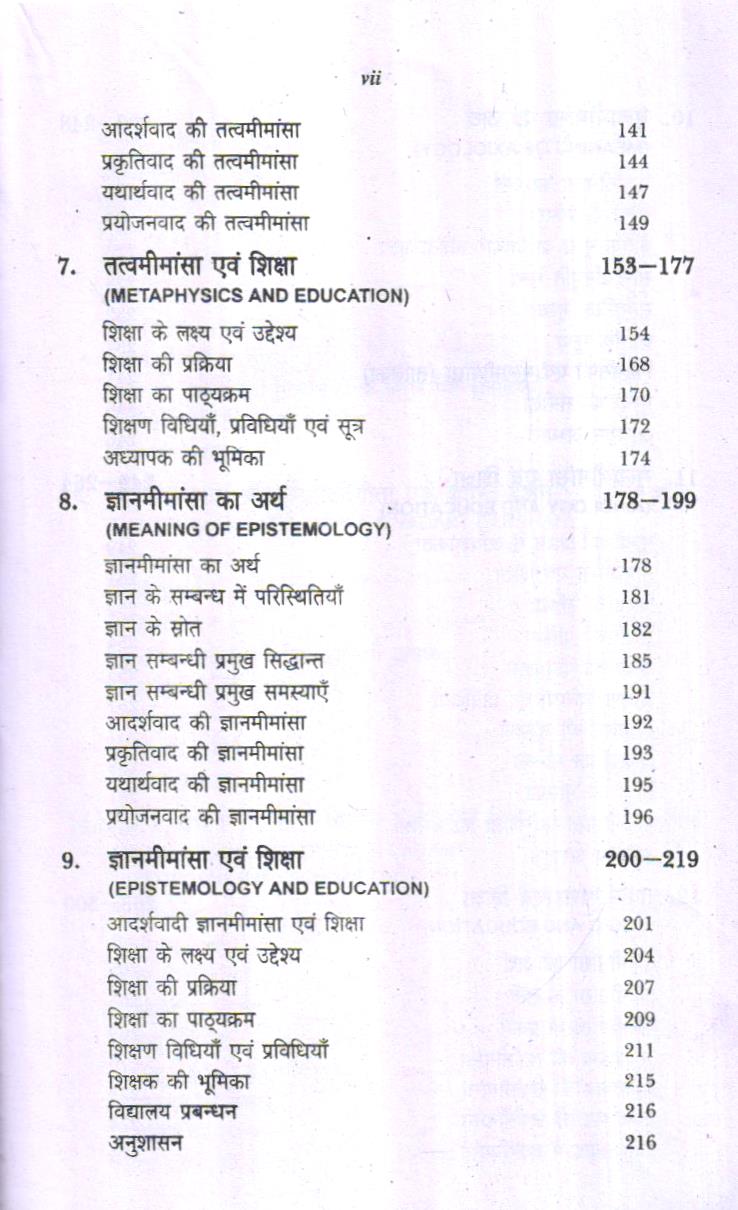
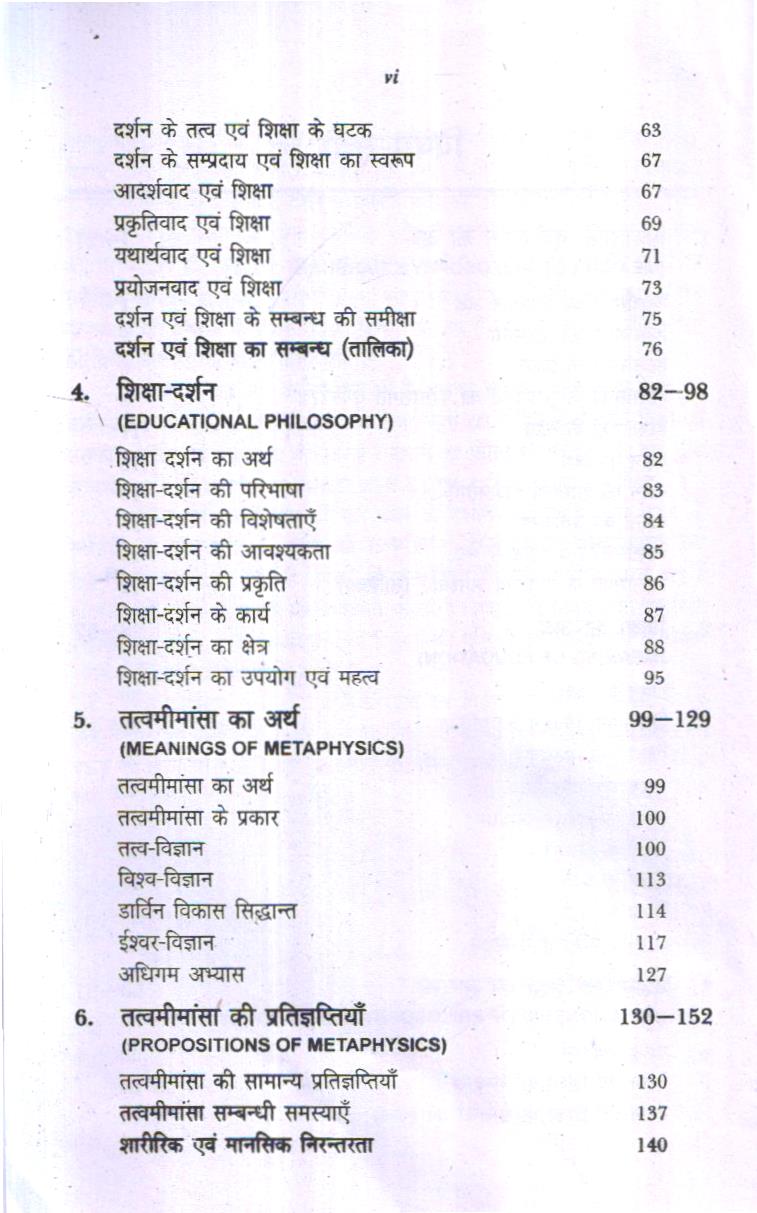
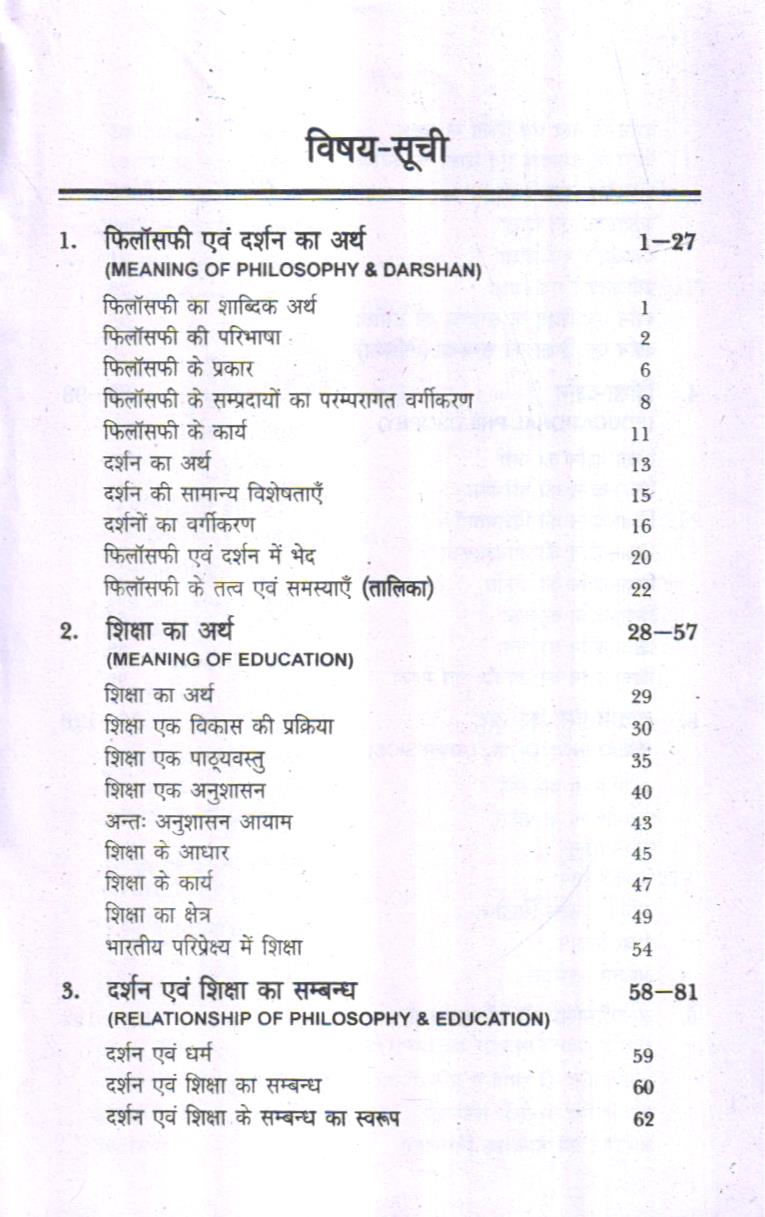
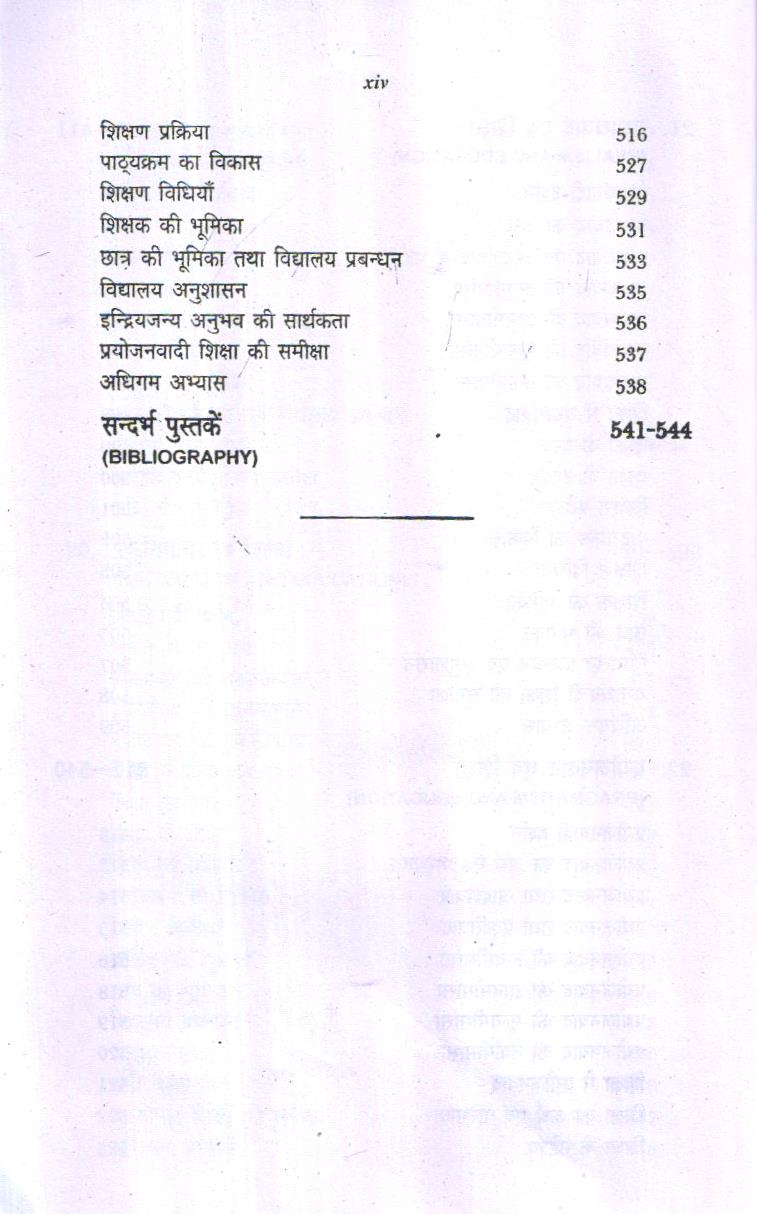
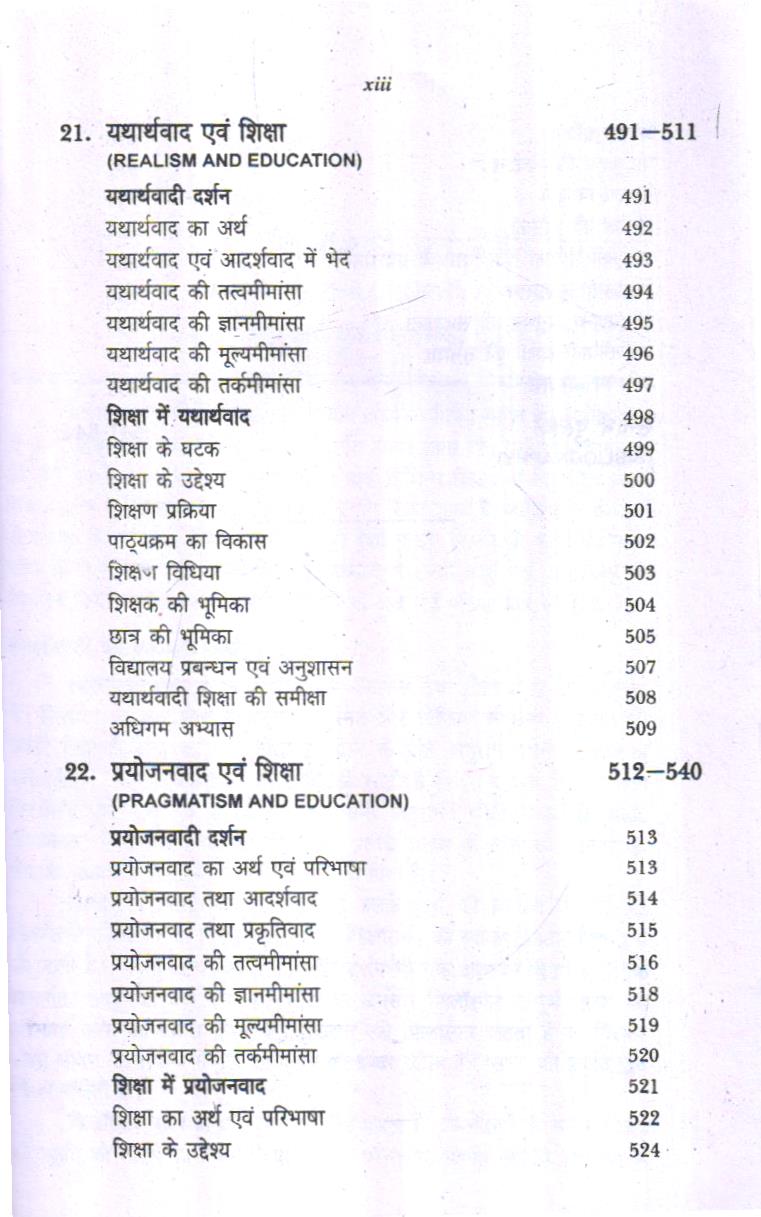
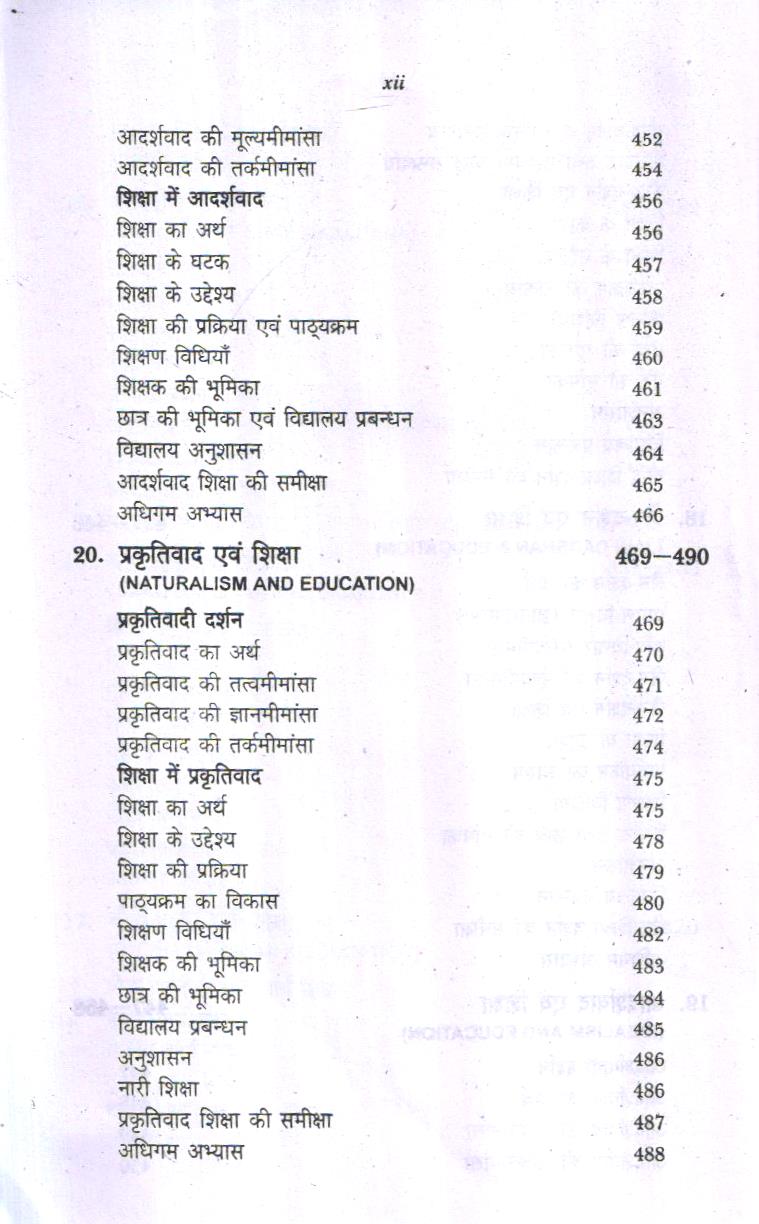
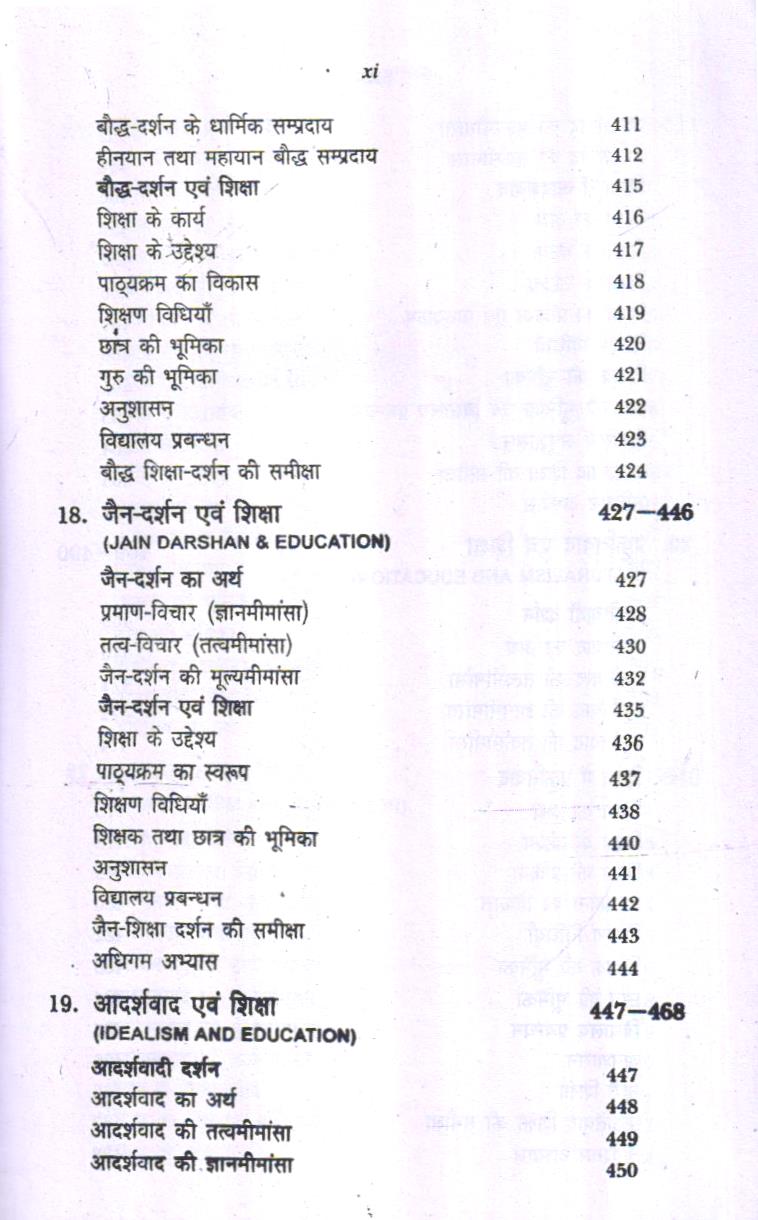




Reviews
There are no reviews yet.